मुहर्रम: इस्लामी नव वर्ष और त्याग का पवित्र महीना
मुहर्रम इस्लामी लूनर कैलेंडर का पहला महीना है। जो हिजरी नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है अरबी में ‘मुहर्रम’ का अर्थ है ‘पवित्र’ या ‘वर्जित’। इस महीने में युद्ध या झगड़े की मनाही रहती है। मुहर्रम को इस्लाम में चार पवित्र महीनों में से एक माना गया है जहाँ संघर्ष-विवाद वर्जित होते हैं। इसी माह का दसवां दिन अशूरा कहलाता है, जिसका महत्व सुन्नी और शीया मुसलमान दोनों के लिए भिन्न है। सुन्नी पक्ष में इस दिन को मूसा (अलैहिस्सलाम) द्वारा लाल सागर को पार करने और इस्राएलियों की रिहाई की याद में रोजा रखकर मनाया जाता है। कई सुन्नी समुदायों में इस मौके पर उत्सव, मेले, विशेष पकवान बनाने और दीवारों पर राख छिड़कने जैसी परंपराएँ भी होती हैं। जबकि शीया मुसलमान अशूरा को पैगंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के नाती इमाम हुसैन (रेह) की 680 ईस्वी में करबला में शहादत की याद में मातम करके मनाते हैं।
करबला का युद्ध: एक ऐतिहासिक त्रासदी
इस्लाम में सुन्नी और शिया शाखाओं के बीच विभाजन की जड़ें पैगंबर मुहम्मद (PBUH) की मृत्यु के तुरंत बाद नेतृत्व के उत्तराधिकार के विवाद में निहित हैं । शिया (शियात अली - अली की पार्टी) पैगंबर के दामाद और चचेरे भाई अली इब्न अबी तालिब को अपना उत्तराधिकारी मानते थे, जबकि सुन्नियों ने अबू बक्र को पहला खलीफा चुना । तीसरे खलीफा, उस्मान की हत्या के बाद अली खलीफा बने, लेकिन उमय्यद कबीले के मुआविया (उस्मान के चचेरे भाई और सीरिया के गवर्नर) के साथ उनके संबंध बिगड़ गए, जिससे पहला फितना (गृहयुद्ध) हुआ । मुआविया ने बाद में अपने बेटे यज़ीद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जो इस्लामी सिद्धांतों का उल्लंघन था, क्योंकि यह वंशानुगत शासन की शुरुआत थी । इमाम हुसैन ने यज़ीद के भ्रष्ट और अनैतिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया ।
युद्ध कब और कहाँ हुआ?
करबला का युद्ध 10 अक्टूबर, 680 ईस्वी को हुआ था, जो इस्लामी कैलेंडर के अनुसार 10 मुहर्रम, 61 हिजरी का दिन था । यह इस्लामी इतिहास की सबसे मार्मिक और निर्णायक घटनाओं में से एक है। यह युद्ध इराक में फरात नदी के पश्चिम में करबला नामक स्थान पर हुआ था ।
किनके बीच हुआ युद्ध?
करबला का युद्ध दो मुख्य पक्षों के बीच लड़ा गया था:
इमाम हुसैन (अ.स.) और उनके साथी: इमाम हुसैन, पैगंबर मुहम्मद (PBUH) के प्यारे पोते और चौथे खलीफा अली के बेटे थे । उनके साथ परिवार के सदस्य और लगभग 70 वफादार साथी थे, जिनमें उनके छह महीने के शिशु अली असगर भी शामिल थे, जिन्हें बेरहमी से शहीद कर दिया गया ।
उमय्यद खलीफा यज़ीद प्रथम की सेना: यह यज़ीद प्रथम (जो 680-683 ईस्वी तक शासन किया) के आदेश पर उबैद अल्लाह द्वारा भेजी गई एक बड़ी सेना थी । इस सेना का नेतृत्व उमर इब्न साद ने किया था, और उनकी संख्या 4,000 से 5,000 के बीच अनुमानित है ।
शिया और सुन्नी मतभेद
धार्मिक आधार मुख्य रूप से पैगंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की मृत्यु के बाद इस्लाम के नेतृत्व (खिलाफत) को लेकर शुरू हुआ था।
नेतृत्व को लेकर मतभेद
शिया मानते हैं कि पैगंबर ने अपने चचेरे भाई और दामाद हजरत अली को अपना असली उत्तराधिकारी (इमाम) घोषित किया था। उनके अनुसार, इस्लाम का नेतृत्व सिर्फ़ पैगंबर के परिवार (अहलेबैत) के हाथ में होना चाहिए। इसलिए वे हजरत अली और उनके वंशजों को इमाम मानते हैं, जिनका आध्यात्मिक और राजनीतिक नेतृत्व सर्वोपरि है।
सुन्नी समुदाय का मानना है कि पैगंबर ने किसी को स्पष्ट उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया और मुसलमानों ने सहमति से अबू बकर को पहला खलीफा चुना। वे नेतृत्व को चुनाव या सहमति से चुने गए खलीफाओं के माध्यम से मानते हैं और पैगंबर के परिवार को विशेष आध्यात्मिक दर्जा नहीं देते।
धार्मिक और विधिक मतभेद
शिया मुसलमान अपने धार्मिक कानून (फिकह) के लिए जाफ़रियाह स्कूल का पालन करते हैं, जो पैगंबर के परिवार की शिक्षाओं पर आधारित है।
सुन्नी मुसलमान चार प्रमुख फिक़ह स्कूलों (हनाफ़ी, मालिकी, शाफ़ई, हनबली) का अनुसरण करते हैं, जो पैगंबर की हदीसों और सहाबा की परंपराओं पर आधारित हैं।
धार्मिक आस्थाएं और प्रथाएं
शिया समुदाय पैगंबर के परिवार (अहलेबैत) को इस्लाम का असली मार्गदर्शक मानते हैं और उनकी पूजा, सम्मान और शहादत को विशेष महत्व देते हैं। मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन की शहादत का शोक मनाना इसका उदाहरण है।
सुन्नी मुसलमान भी इमाम हुसैन और अहलेबैत का सम्मान करते हैं, लेकिन वे इस विषय में शिया की तरह धार्मिक रस्मों और मातम की परंपराओं को नहीं अपनाते।
सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव
यह मतभेद केवल धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक हितों से भी जुड़े रहे हैं। इतिहास में कई बार दोनों समुदायों के बीच सत्ता संघर्ष, क्षेत्रीय और जातीय मतभेद भी जुड़े।
आज भी यह मतभेद कई मुस्लिम देशों में राजनीतिक संघर्ष और साम्प्रदायिक तनाव का कारण बनते हैं।
युद्ध क्यों हुआ? कारण और उद्देश्य
युद्ध का मूल कारण इमाम हुसैन का यज़ीद के शासन को नैतिक आधार पर स्वीकार करने से इनकार करना था। यज़ीद को अक्सर मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा अधर्मी और अनैतिक शासक के रूप में चित्रित किया जाता है । इमाम हुसैन का उद्देश्य राजनीतिक लाभ या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं था, बल्कि वे अपने दादा (पैगंबर मुहम्मद) के उम्माह में सुधार लाना चाहते थे। उनका लक्ष्य न्याय स्थापित करना और बुराई को रोकना था । करबला में उनकी लड़ाई सत्य और असत्य, न्याय और अत्याचार, आस्था और भ्रष्टाचार के बीच शाश्वत संघर्ष का प्रतीक बन गई । उन्होंने असहनीय प्यास और पीड़ा के बावजूद अधीनता के बजाय शहादत को चुना, जो उनके अडिग सिद्धांतों को दर्शाता है ।
करबला का गहरा प्रभाव
इस युद्ध ने उमय्यद राजवंश के खिलाफ विरोध को मजबूत किया, जिसे लगभग 70 साल बाद एक खूनी विद्रोह में उखाड़ फेंका गया । यह घटना शिया समुदाय को एक विशिष्ट संप्रदाय के रूप में क्रिस्टलीकृत करने में सहायक थी और आज भी उनकी धार्मिक पहचान का एक अभिन्न अंग बनी हुई है । करबला की त्रासदी ने पूरे मुस्लिम समुदाय को झकझोर दिया और कुछ सुन्नी मुसलमान भी इसे याद करते हैं, हालांकि उनके अनुष्ठान शियाओं से भिन्न हो सकते हैं ।
करबला सिर्फ एक सैन्य हार या राजनीतिक हत्या नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा निर्णायक क्षण था जिसने एक राजनीतिक असहमति को एक स्थायी धार्मिक और सांप्रदायिक पहचान में बदल दिया। इमाम हुसैन का बलिदान शिया इस्लाम के केंद्रीय सिद्धांत का आधार बन गया, जिसने उनके धार्मिक अनुष्ठानों, विश्वासों और सामाजिक संरचनाओं को आकार दिया। यह घटना केवल इतिहास का एक बिंदु नहीं, बल्कि शिया पहचान का एक जीवित, विकसित होता हुआ प्रतीक है, जो न्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष के शाश्वत संदेश को वहन करता है।
इमाम हुसैन का यह कथन कि "मैं बुराई फैलाने या दिखावा करने के लिए नहीं उठा हूं। मैं केवल अपने दादा (पैगंबर मुहम्मद) के उम्माह में सुधार लाना चाहता हूं। मैं अच्छाई का आदेश देना चाहता हूं और बुराई को रोकना चाहता हूं" , इस घटना के कालातीत नैतिक और सामाजिक संदेश को दर्शाता है। मुहर्रम का वार्षिक स्मरण केवल अतीत को याद करना नहीं है, बल्कि वर्तमान में अन्याय, भ्रष्टाचार और उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने के लिए एक सक्रिय आह्वान है । यह धार्मिक अनुष्ठानों को समकालीन सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता से जोड़ता है, जिससे मुहर्रम की प्रासंगिकता हर युग में बनी रहती है। यह दर्शाता है कि इतिहास केवल याद रखने के लिए नहीं, बल्कि वर्तमान को सूचित करने और भविष्य को आकार देने के लिए है, जिससे यह एक गतिशील और जीवंत परंपरा बन जाती है।
मुहर्रम की वैश्विक परंपराएँ: शोक और स्मरण
मुहर्रम का पालन मुस्लिम समुदाय के भीतर, विशेष रूप से शिया और सुन्नी संप्रदायों के बीच, काफी भिन्न होता है।
शिया मुसलमानों द्वारा मुहर्रम का पालन
शिया मुसलमानों के लिए मुहर्रम गहन शोक और स्मरण का समय है, विशेष रूप से पहले दस दिनों के दौरान, जो आशूरा पर समाप्त होता है । यह इमाम हुसैन और पैगंबर के परिवार के सदस्यों की करबला में हुई शहादत के लिए गहरा दुख व्यक्त करने का एक तरीका है ।
आशूरा: शोक का चरम दिन
10 मुहर्रम, जिसे आशूरा के नाम से जाना जाता है, शिया मुसलमानों के लिए शोक का मुख्य दिन है । इसी दिन इमाम हुसैन, उनके परिवार और साथियों को करबला में बेरहमी से शहीद कर दिया गया था ।
मजलिस, मातम और ताज़िया
शोक सभाएँ, जिन्हें मजलिस कहा जाता है, घरों, मस्जिदों और सामुदायिक केंद्रों में आयोजित की जाती हैं । इन सभाओं में धार्मिक विद्वान और वक्ता करबला की कहानी सुनाते हैं, जिसमें इमाम हुसैन के साहस, मूल्यों और बलिदान पर प्रकाश डाला जाता है । इन सत्रों में शोकगीतों (मर्सिया और नौहा) का पाठ और धार्मिक उपदेश (बयान) शामिल होते हैं । भागीदार अपनी छाती पीटकर (मातम, लत्म, सीना-ज़नी) इमाम हुसैन के दर्द में शामिल होते हैं, जो दुख और प्रेम की एक तीव्र अभिव्यक्ति है ।
शोक जुलूस, जिन्हें दस्ता, जुलूस या मौकिब कहा जाता है, वार्षिक रूप से सड़कों पर निकलते हैं, विशेषकर आशूरा पर । इन जुलूसों में शोकगीत गाए जाते हैं और कभी-कभी आत्म-यातना भी की जाती है । ये जुलूस आमतौर पर स्थानीय हुसैनीया (शिया सभा स्थल) से शुरू और समाप्त होते हैं ।
भारत और दक्षिण एशिया के अन्य हिस्सों में, इमाम हुसैन की कब्र या ताबूत की प्रतिकृतियाँ, जिन्हें ताज़िया कहा जाता है, ले जाई जाती हैं, जिन्हें अंततः दफनाया या विसर्जित किया जाता है । यह विसर्जन प्रथा संभवतः स्थानीय हिंदू प्रभावों को दर्शाती है, जो धार्मिक अनुष्ठानों में सांस्कृतिक अनुकूलन का एक उदाहरण है। ईरान में, ताज़िया करबला के नाटकीय पुनर्मंचन को भी संदर्भित करता है, जिसे ताज़ियाह या शबीह-ख्वानी के नाम से जाना जाता है ।
ईरान में मुहर्रम के दौरान कई अन्य विशिष्ट अनुष्ठान भी प्रचलित हैं। इनमें नखलगोज़ारी शामिल है, जो यज़्द प्रांत में प्रचलित एक गंभीर समारोह है, जहाँ 'नखल' (खजूर का पेड़) इमाम हुसैन के ताबूत का प्रतीक है । तब्रिज़ में शाह हुसैन गौयान एक सैन्य परेड जैसा जुलूस है, जो इमाम हुसैन के साथ युद्ध में खड़े होने की तैयारी का प्रतीक है । गिलान में कर्बज़ानी पश्चाताप और खेद का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जबकि लोरेस्तान प्रांत में गेल माली में प्रतिभागी अपने सिर और शरीर पर कीचड़ और धूल रगड़ते हैं, जो किसी प्रियजन के खोने के लिए निराशा और दुख का प्रतीक है । ये प्रथाएं दर्शाती हैं कि इस्लामी धार्मिक अनुष्ठान पूरी तरह से एकरूप नहीं होते, बल्कि स्थानीय सांस्कृतिक संदर्भों और पूर्व-मौजूदा परंपराओं के साथ बातचीत करते हुए विकसित होते हैं।
आत्म-यातना पर विवाद
आत्म-यातना के अत्यधिक रूप, जिसमें रक्तपात शामिल है (जैसे तलवारों से आत्म-यातना या जंजीर-ज़नी), शियाओं के बीच अत्यधिक विवादास्पद हैं । कई शिया विद्वानों द्वारा इनकी निंदा की जाती है, और कुछ शिया समुदायों में ये अवैध भी हैं । रक्त दान को कभी-कभी आत्म-यातना के एक सुरक्षित और परोपकारी विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया जाता है ।
सुन्नी मुसलमानों द्वारा मुहर्रम का पालन
सुन्नी मुसलमान भी मुहर्रम को महत्व देते हैं, लेकिन उनके अनुष्ठान शियाओं से भिन्न होते हैं ।
आशूरा का उपवास और अन्य शुभ घटनाएँ
सुन्नी मुसलमानों के लिए, आशूरा (10 मुहर्रम) पैगंबर मूसा (मोसेस) द्वारा लाल सागर को पार करने और इस्राएलियों के फिरौन से उद्धार का प्रतीक है । इस दिन नूह की किश्ती भी उतरी थी, आदम को अल्लाह ने माफ किया था, और यूसुफ को जेल से रिहा किया गया था । पैगंबर मुहम्मद ने आशूरा पर उपवास करने को प्रोत्साहित किया, और कई सुन्नी मुसलमान स्वेच्छा से 9वें और 10वें या 10वें और 11वें मुहर्रम को उपवास करते हैं । यह उपवास पापों के प्रायश्चित और अल्लाह के प्रति कृतज्ञता के रूप में देखा जाता है । पैगंबर ने यहूदियों से खुद को अलग करने के लिए 9वें मुहर्रम को भी उपवास करने की सलाह दी थी ।
कुछ सुन्नी समुदायों में, आशूरा उत्सव, अलाव और विशेष व्यंजनों के साथ मनाया जाता है, हालाँकि कुछ सुन्नी विद्वानों ने ऐसी प्रथाओं की आलोचना की है ।
भेदभाव और साझा सम्मान
सुन्नी इस्लाम में आशूरा को कृतज्ञता के दिन के रूप में देखा जाता है, जबकि शिया इसे गहन शोक के दिन के रूप में मनाते हैं । यह केवल अनुष्ठानों में अंतर नहीं है, बल्कि घटना के अंतर्निहित अर्थ और भावनात्मक प्रतिक्रिया में एक मौलिक अंतर है। ऐतिहासिक रूप से, उमय्यद खलीफा अब्द अल-मलिक इब्न मरवान के तहत, आशूरा को हुसैन के स्मरण का मुकाबला करने के लिए एक उत्सव सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया गया था । यह दिखाता है कि धार्मिक व्याख्याएं कैसे राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि, दक्षिण एशिया में, कुछ सुन्नी आधुनिक समय तक शिया अनुष्ठानों में भाग लेते है, जो साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है ।
सूफी परंपरा में मुहर्रम
सूफीवाद में भी मुहर्रम के अनुष्ठान दिखाई देते हैं, लेकिन करबला को त्रासदी के बजाय इमाम हुसैन और उनके साथियों के शाश्वत जीवन के उत्सव के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने अल्लाह में आत्म-बलिदान किया । यह सूफी दर्शन में 'फ़ना' (आत्म-विनाश) के विचार से जुड़ा है।
किन मुस्लिम देशों में मुहर्रम मनाया जाता है?
मुहर्रम का शोक विशेष रूप से शिया बहुल देशों और समुदायों में व्यापक रूप से मनाया जाता है । इन क्षेत्रों में, यह एक प्रमुख सार्वजनिक धार्मिक आयोजन है, जो उनकी सांप्रदायिक पहचान का एक केंद्रीय बिंदु है।
प्रमुख शिया बहुल देश और उनके अनुष्ठान
ईरान और इराक में, मुहर्रम के पहले दस दिनों के दौरान प्रमुख शिया शहरों में जुलूसों के साथ शोक अनुष्ठान चरम पर होते हैं । इराक में करबला में इमाम हुसैन के मकबरे की तीर्थयात्रा भी की जाती है । लेबनान, बहरीन और अजरबैजान जैसे देशों में भी शिया समुदाय द्वारा गहन शोक मनाया जाता है । ईरान में ताज़िया (नाटकीय पुनर्मंचन), नखलगोज़ारी, शाह हुसैन गौयान, कर्बज़ानी और गेल माली जैसे विशिष्ट अनुष्ठान प्रचलित हैं ।
भारत और दक्षिण एशिया में मुहर्रम
भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे दक्षिण एशियाई देशों में भी मुहर्रम मनाया जाता है । इन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी की विविधता के कारण पालन के तरीके भी विविध हैं। भारत में, यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार है जिसे मुस्लिम मनाते हैं । यह मुख्य रूप से शिया इस्लाम में महत्वपूर्ण है, हालांकि सुन्नी मुसलमान भी इस महीने को श्रद्धा के साथ मनाते हैं । भारत में यह राष्ट्रीय सार्वजनिक अवकाश नहीं है, लेकिन जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, जहाँ शिया मुस्लिम आबादी अधिक है, स्थानीय प्रशासन आशूरा के दिन छुट्टी घोषित कर सकता है । केरल के मप्पिला मुस्लिम, जो राज्य की 25% आबादी का गठन करते हैं, इमाम हुसैन की दुखद मृत्यु की याद में इसे मनाते हैं । दक्षिण एशिया में ताज़िया जुलूस एक आम प्रथा है, जिसमें इमाम हुसैन के मकबरे की प्रतिकृतियां ले जाई जाती हैं ।
वहाबवाद का दृष्टिकोण
सऊदी अरब में प्रचलित वहाबी विचारधारा, जो सुन्नी इस्लाम की एक रूढ़िवादी शाखा है, संतों के निधन या जन्म के लिए किसी भी प्रकार की सभा को मूर्ति पूजा के समान मानती है । वहाबी दृष्टिकोण के अनुसार, केवल दो इस्लामी त्योहार (ईद अल-फितर और ईद अल-अधा) मनाए जाने चाहिए, क्योंकि पैगंबर ने केवल इन्हीं दो त्योहारों को अलग किया और उनका आदेश दिया । वे किसी भी अन्य "त्योहार" या शोक समारोह को बिदाह (नवाचार) मानते हैं, जो इस्लामी परंपरा में बाद में जोड़ा गया है और पैगंबर की शिक्षाओं के अनुरूप नहीं है । इब्न तैमिया (एक सुन्नी न्यायविद) ने आशूरा पर शोक और उत्सव दोनों को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनका तर्क था कि पैगंबर ने इनमें से किसी का भी अभ्यास नहीं किया था, हालांकि उन्होंने उपवास को प्रोत्साहित किया । इस प्रकार, सऊदी अरब में शियाओं द्वारा मनाए जाने वाले गहन शोक अनुष्ठान (जैसे मातम, ताज़िया, आत्म-यातना) को वहाबी दृष्टिकोण के तहत अस्वीकार्य माना जाता है ।
सऊदी अरब में मुहर्रम के पालन का अभाव केवल एक सांस्कृतिक पसंद नहीं है, बल्कि यह देश की आधिकारिक धार्मिक विचारधारा (वहाबवाद) का प्रत्यक्ष परिणाम है। वहाबवाद की सख्त व्याख्याएं उन अनुष्ठानों को अस्वीकार करती हैं जिन्हें वे इस्लामी परंपरा में बाद के नवाचार या अत्यधिक veneration मानते हैं। यह दर्शाता है कि राज्य की धार्मिक नीति कैसे धार्मिक पालन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति को आकार दे सकती है और कुछ संप्रदायों (जैसे शिया) की प्रथाओं को हाशिए पर धकेल सकती है, भले ही वे वैश्विक मुस्लिम समुदाय के लिए महत्वपूर्ण हों।
मुहर्रम का ऐतिहासिक सफर: शुरुआत से आज तक
मुहर्रम का इतिहास इस्लाम के उदय से भी पहले का है। इस्लाम के आगमन से पहले भी मुहर्रम चार पवित्र महीनों में से एक था जिसमें युद्ध निषिद्ध था । यह इसकी पूर्व-इस्लामी पवित्रता को दर्शाता है। पैगंबर मुहम्मद (PBUH) ने मदीना आने से पहले भी आशूरा पर उपवास किया था । जब उन्होंने यहूदियों को उपवास करते देखा, तो उन्होंने मुसलमानों को भी ऐसा करने का निर्देश दिया, जिससे यह सुन्नत बन गया । पैगंबर ने बाद में यहूदियों से खुद को अलग करने के लिए 9वें मुहर्रम को भी उपवास करने की सलाह दी । 1 मुहर्रम को दूसरे खलीफा उमर की मृत्यु (634-644 ईस्वी) का भी स्मरण किया जाता है, जिसके लिए कुछ सुन्नी रैलियां निकालते हैं । 16 मुहर्रम को, पैगंबर मुहम्मद ने यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद को किबला (नमाज़ की दिशा) के रूप में स्थापित किया था, जिसे बाद में मक्का में काबा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ।
करबला के बाद अनुष्ठानों का विकास
करबला के लिए शोक इसकी महिला जीवित बची हुई सदस्यों, विशेष रूप से इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब के साथ शुरू हुआ, और समय के साथ विशिष्ट अनुष्ठानों में विकसित हुआ जिसने शिया पहचान को परिभाषित करने में मदद की । उमय्यद काल (661-750 ईस्वी) के दौरान, आशूरा को मूसा के उद्धार जैसे शुभ घटनाओं से जोड़ा गया और कभी-कभी इसे उत्सव के रूप में भी मनाया गया, संभवतः हुसैन के स्मरण का मुकाबला करने के लिए । यह राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक व्याख्याओं के हेरफेर को दर्शाता है।
बुयिद राजवंश (934-1062 ईस्वी) के तहत, सार्वजनिक शोक अनुष्ठानों को वैधता मिली और वे शिया समुदायों में अधिक व्यापक हो गए । सफ़वीद युग (1576 - लगभग 1736 ईस्वी) ने ईरान में ताज़िया (नाटकीय पुनर्मंचन) और नखलगोज़ारी जैसे कई विशिष्ट मुहर्रम अनुष्ठानों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।
आधुनिक समय में, मुहर्रम के अनुष्ठानों में विविधता जारी है। आत्म-यातना के अत्यधिक रूपों पर विवाद बना हुआ है, और रक्त दान जैसे परोपकारी विकल्प सामने आए हैं । सूफी परंपरा में, करबला को त्रासदी के बजाय इमाम हुसैन और उनके साथियों के शाश्वत जीवन के उत्सव के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने अल्लाह में आत्म-बलिदान किया । यह सूफी दर्शन में 'फ़ना' (आत्म-विनाश) के विचार से जुड़ा है।
आज भी, मुहर्रम न्याय, बलिदान और नैतिक साहस के प्रतीक के रूप में प्रासंगिक बना हुआ है । यह केवल अतीत की घटना का स्मरण नहीं है, बल्कि अन्याय, उत्पीड़न और नैतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने की स्थायी प्रासंगिकता की याद दिलाता है।
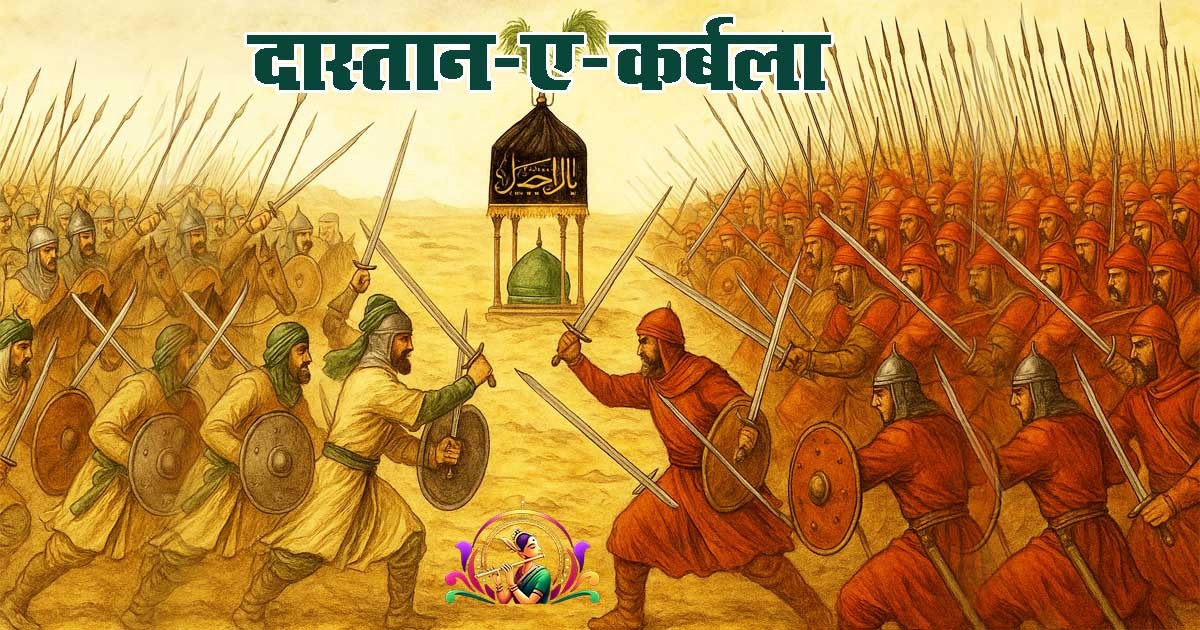




No comments yet.